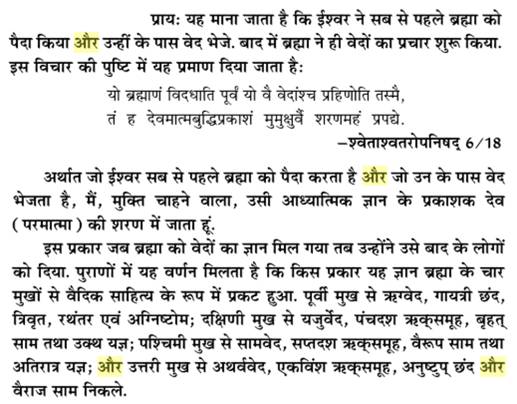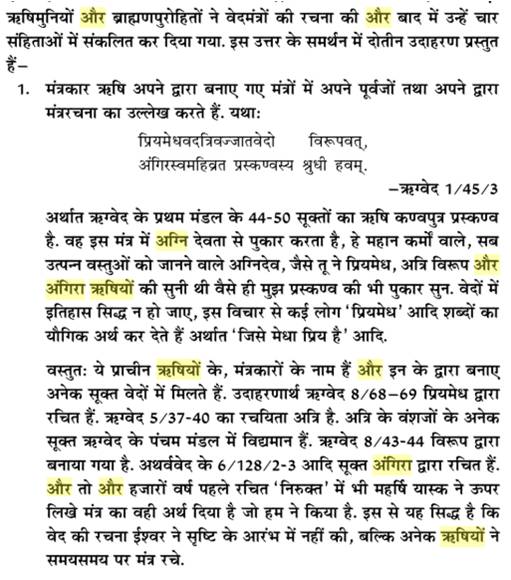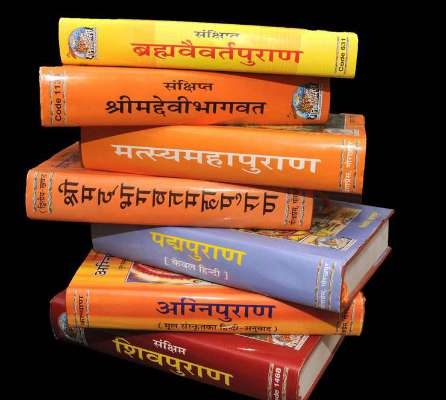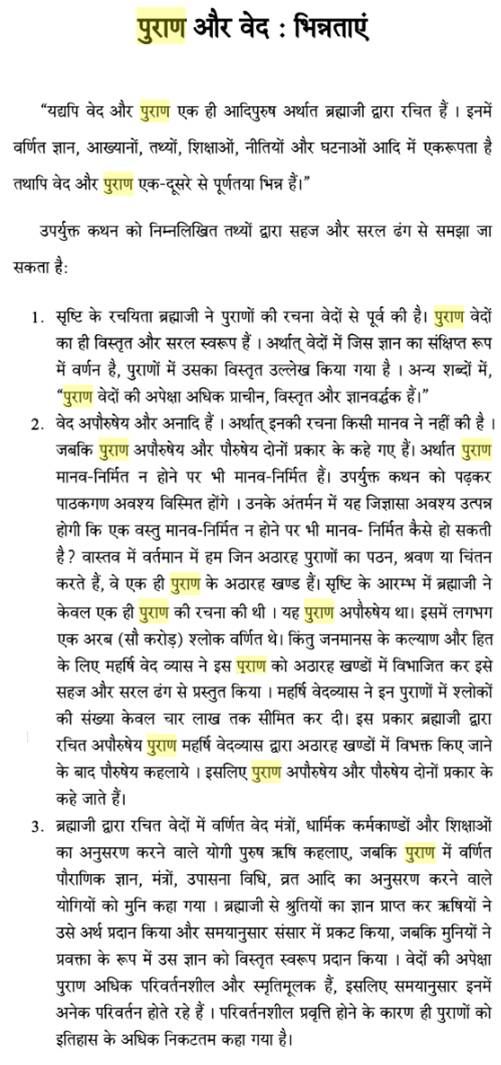डॉ. संदीप कोहली… कीबोर्ड के पत्रकार
वैदिक साहित्य में वनस्पतियों के उल्लेख है-किंशुक, करञ्ज, खदिर, दूर्वा, पिप्पल, कमल,आँवला, सेमल, गोधूम मसूर, बेर, अपामार्ग, अर्क, अश्वत्थ, तिल, अर्जुन, तिलपिप्पली, पृश्नपर्णी, विल्ब, उदुम्बर, इक्षु, ल्णक्षा सहदेवी, सोम, मुञ्ज, गुग्गुल आदि- वैदिक काल में वनस्पतियों का विशेष महत्व था। वनस्पतियां जीवनदायिनी मानी जाती थी। शरीर में हुए रोगों को दूर करती थीं। यजुर्वेद- औषधियों और वनस्पतियों से शान्ति-प्राप्ति की कामना करता है। इससे यही सिद्ध होता है कि मानव जीवन वनस्पतियों पर आधारित रहा है। वेदों में जिन प्रमुख वनस्पतियों का उल्लेख है उसमें से एक है ‘सोम’। और इसी सोम से बनाया जाता था ‘सोमरस’। वही सोमरस जिसका सेवन देवता किया करते थे। देवताओं से जुड़े हर ग्रंथ, कथा, संदर्भ में देवगणों को सोमरस का पान करते हुए बताया जाता है। इन समस्त वर्णनों में जिस तरह सोमरस का वर्णन किया जाता है। अब प्रश्न उठता है- क्या सोमरस मदिरा (शराब) थी या औषधि ।
क्या है सोमरस- सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि सोमरस मदिरा (शराब) की तरह कोई मादक पदार्थ नहीं है। हमारे वेदों में सोमरस का विस्तृत विवरण मिलता है। विशेष रूप से ऋग्वेद में तो कई ऋचाएं विस्तार से सोमरस बनाने और पीने की विधि का वर्णन करती हैं।
सोम एक रस है- रस शब्द का सर्वप्रथम व्यवहार वेदों में हुआ। ऋग्वेद में रस शब्द का प्रयोग कभी मधु, कभी गौ-क्षीर और कभी सोमरस को प्रकट करने के लिए हुआ है। एक स्थल पर रस को उदक के पर्याय के रूप में ग्रहण किया गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वेदों में “रस” शब्द से तात्पर्य किसी भी तरलपदार्थ से है और वह “जल” भी हो सकता है।
अथर्ववेद में रस शब्द से तात्पर्य वनस्पतियों के रस से है । वहाँ वनस्पतियों के रस में जलों के रस के मिलने की कामना की गयी है । इसी संहिता के एक अन्य मन्त्र में जलों के रसको वनस्पतियों के रस से पहले उत्पन्न माना गया है। परन्तु सभी वनस्पतियों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है “सोमरस के अर्थ में रस का प्रयोग।”
सोम हिमालय पर्वत पर प्राप्त होने वाली एक लता है जिसको कूटने के बाद निचोड़कर उसका रस निकाला जाता हे और देवतागण उसका पान करते हैं। यह सोम रस वैदिक देवताओं कासबसे प्रिय पेय था। ऋग्वेद में सोमरस का अत्यधिक उत्कृष्ट वाणी में स्तवन (स्तुति) किया गया है।
सोम संसार को धारण करने वाला, इन्द्रिय पोषक रस को धारण करता हुआ, उत्तम वीरता प्रदान करने वाला और हिंसा से रक्षा करने वाला है । यह सोम अग्नि, वायु और सूर्य इन तीनों रूपों को धारण करने वाला है। सोम की सामर्थ्य इसकी इस विशेषता से ही है कि संसार का प्रत्येक जीव सोम के तेज से उत्पन्न होता है और यह जगत् इसके आश्रित है। यह सोम रस आरम्भिक काल में देवताओं के द्वारा स्फूर्तिदायक पेय के रूप में ग्रहण किया जाता रहा होगा क्योंकि वेद में कुछ ऐसे उद्धरण प्राप्त होते हैं जिनमें देवता लोग सोम को पाने के लिए प्रायः उनकी मंत्रों और स्तुतियों से प्रार्थना करते थे जिस प्रकार मल्लाह नाव चलाता है उसी प्रकार यह सोम यज्ञ में यथार्थ वचन रूप स्तुतियों को प्रेरित करता है। यह सोम चेतना को आत्मसात् कर लेता है । जिस प्रकार रथी अपने अश्व को चलाता है उसी प्रकार यह सोम अपनी तरंगों को चलाता है। सोम को कहीं विश्वस्रष्टा, क्रान्तकर्मा, रक्षक एवं आनन्ददायक के रूप में वर्णित किया गया है।
इस प्रकार सोम के अर्थ में रस का प्रयोग विशिष्ट हो गया। सोमरस का आस्वाद अपूर्व था। इसमें कुछ ऐसी विशेषतायें थीं, जिनके कारण उसके पान करने से विचित्र आनन्द की प्राप्ति होती थी, साथ ही शरीर और मन में स्फूर्ति तथा मद का संचार होता था। ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं में वाणी के लिए प्रयुक्त स्वादु, मधु आदि विशेषणों का प्रयोग इस विचार को प्रमाणित करता है कि रस के लिये वाक् शब्द के प्रयोग का भी वैदिक साहित्य में विवरण उपलब्ध होता है-
वचः स्वादो स्वादीयो रुद्राय वर्धनम् ।। ‘अर्थात् रुद्र को प्रसन्न करने के लिये स्वादु से भी स्वादु वचन। इसके अतिरिक्त ‘पिबत्वस्य गिर्वणः’, ‘मध्व ऊषु मधुयुवा रुद्रा सिषक्तिं पिप्युषी, वाचा वदामि’मधुमद् भूयासं मधुसन्दृशः’,’ तथा ‘वाचों मधु पृथिवि! छेहि मह्यम्” आदि से यहस्पष्ट हो जाता है कि रस के अर्थ में ‘वाक्’ का प्रयोग किया जाता है
ऋग्वेद में उल्लेखित है- “जो पुरुष पवमान ऋचाओं (सोमयुक्त) के रूप में ऋषियों द्वारा सम्भृत रस का पान करता है, वह पवित्र और स्वादिष्ट अन्न का आनन्द लेता है उस वेद वाणी के लिए देवी सरस्वती दूध, घृत और सोम का दोहन करती हैं। यहाँ ‘पावमान’ शब्द सोम के लिए प्रयुक्त है ।
भौतिक गुणों के साथ आध्यात्मिकता का समावेश- सोम एक प्रकार का भौतिक रस है। परन्तु जब इसका प्रयोग आध्यात्मिक रूप में किया जाता है तो यह विश्वव्यापक और अमरता को प्राप्त कर लेता है। जहां भौतिक रस के रूप में यह केवल मानवीय है, वहीं अध्यात्म के रूप में दैवीय स्पर्श से अलंकृत हो जाता है। रस के इन दोनों ही रूपों से सम्बन्धित मन्त्र ऋग्वेद में सोम की स्तुतियों में प्राप्त होते हैं ।
उपनिषदों में जिस प्रकार वेदों की अनेक भौतिक कल्पनाओं को सूक्ष्म आध्यात्मिक रूप दे दिया गया उसी प्रकार रस का भी आध्यात्मिक रूपान्तर हुआ। जहां वेदों में रस केवल मधु या सोमरस अथवा दुग्ध का ही अर्थ देता रहा। वहीं उपनिषदों में इनके मूल स्थित स्वाद की भावना का आधार लेकर यही रस मुख्यार्थ का बाधक होकर प्राणस्वरूपमाना जाने लगा। दूसरे शब्दों में उपनिषदों में रस द्रव्य के अर्थ में तो नहीं परन्तु द्रव्य-जनितशक्ति और आनन्द के रूप में प्रयुक्त हुआ । इसके अतिरिक्त न केवल द्रव्य-जनितशक्ति के रूप में बल्कि इससे भी सूक्ष्मतर रूप में तन्मात्राओं के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।
वृहदारण्यक उपनिषद् में ‘प्राणो वा अंगानां रसः” कहकर रस को सार भूततत्त्व कहा गया है । तैत्तिरीय उपनिषद् में स्वयं ब्रह्म को ही रस स्वरूप कहा गया है ।वह अर्थात् ब्रह्म रस स्वरूप है ।
शक्ति, तन्मयता और आनन्द का समावेश- उपर्युक्त विवरण के अतिरिक्त ‘आनन्द’ तथा ‘काम’ के रूप में भी रस के अर्थका विकास वैदिक युग में ही हुआ । आनन्द शब्द सम्पूर्ण ऋग्वेद में दो बार प्राप्त होताहै । वह भी सोम की स्तुति में ही।एक मन्त्र के अनुसार ऋत्विज जन सोम की स्तुतिमें छन्दोबद्ध वर्णन करते हुये सोम लता को पत्थर पर पीसने से उत्पन्न ध्वनि से आनन्द काअनुभव करते थे । इसका अभिप्रायः यह हो सकता है कि जब ऋत्विज् जन सोम लताको पत्थर पर पीसते थे और साथ-साथ सोम की स्तुति में मंत्रों का पाठ भी करते थे तबपीसने से उत्पन्न ध्वनि और मंत्रों के उच्चारण से एक आनन्द प्राप्त होता था ।
आनन्द की प्रकृति को समझने से “कामस्य यत्राप्ताः कामाः इस विचार कोभी स्थान प्राप्त होता है । इसके अनुसार व्यक्ति की सभी इच्छाओं के पूर्ण होने सेअथवा सभी इच्छाओं से रहित हो जाने से परम आनन्द की प्राप्ति होती है 12 काम(इच्छा) और रस की इस दशा का वर्णन अर्थर्ववेद में इस प्रकार प्राप्त होता है –
“अकामोधीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्च नोनः”
अर्थात् वह आत्मा अकाम् अर्थात्इच्छाओं से रहित, धीर, अमृत, स्वयं उत्पन्न; अपने रस से स्वतः तृप्त रहता है। अतः कहा जा सकता है कि सोम रस के संसर्ग से रस की अर्थ परिधि में क्रमशः शक्ति, तन्मयता और अन्त में आनन्द का समावेश हो गया ।
सोम और सुरा में अंतर

हमारे धर्मग्रंथों में मदिरा के लिए मद्यपान शब्द का उपयोग हुआ है, जिसमें मद का अर्थ अहंकार या नशे से जुड़ा है। इससे ठीक अलग सोमरस के लिए सोमपान शब्द का उपयोग हुआ है, जहां सोम का अर्थ शीतल अमृत बताया गया है।
वैदिककाल में मद्यपान का प्रचलन- वैदिक कालीन समाज कृषि प्रधान था। और वैदिक काल में सोम और सुरा का प्रचलन था। सोमयज्ञो में सोम एवं सोत्रामणी में सुरापान किया जाता था। वैदिक आर्य अपने इष्ट देवता इन्द्र को सोम व सुरा अर्पित करने के बाद पीते थे।
ऋग्वेद में दो प्रकार के मादक पेयों सोम और सुरा का उल्लेख है- सोम पुरोहितों और देवताओं द्वारा ग्रहण करने वाला पेय पदार्थ था। सुरा जन-साधारण द्वारा उपयोग किया जाने वाला पेय पदार्थ था। ‘ऋग्वेद‘ में मद्य का एक नाम ‘मत्सर भी है। इसका प्रसिद्ध अर्थ लोभ है।
ऋग्वेद में सोम और सुरा में फर्क बताया गया है– ऋग्वेद में सुरा की घोर निंदा करते हुए कहा गया है-
हृत्सु पीतासो युध्यन्ते दुर्मदासो न सुरायाम्।।
अर्थात: सुरापान करने या नशीले पदार्थों को पीने वाले अक्सर युद्ध, मार-पिटाई या उत्पात मचाया करते हैं।
‘तैत्तिरीय ब्राह्मण‘ (1-3-3-3) का कहना है:
एतद् वै देवानां परममन्नं यत्सोम:, एतन्मनुष्याणां यत्सुरा.
अर्थात: सोम देवताओं का परम अन्न है और सुरा मनुष्यों का परम अन्न है.
‘शतपथब्राह्मण‘ (12-7-3-94) कहता है:
यशो हि सुरा.
अर्थात: सुरा से यश फैलता/मिलता है
‘तैत्तिरीय ब्राह्मण‘ ( 1-3-3-4) कहता है:
पुमान् वै सोम: स्त्री सुरा (तैत्तिरीय ब्राह्मण 1-3-3-4)
अर्थात: सोम को पुंलिंग (पुरुष) और सुरा (स्त्री) को उस की पत्नी कहा गया है।
सौत्रामणी नामक यज्ञ में तो सुरापान का विधान है—
सौत्रामण्यां सुरां पिबेत्. शतपथब्राह्मण (12-8-1-2)
इसीलिए सौत्रामणी यज्ञ को सुरावाला (सुरावान्) यज्ञ कहा है—
सुरावान् वा एष बहिंषद् यज्ञो यत् सौत्रामणी।
देवताओं के लिए ‘सुर‘ शब्द का प्रयोग होता है, जो उन के सुरापान करने के कारण ही अस्तित्व में आया है. आप्टे ने अपने कोश में ‘सुर’ शब्द का अर्थ बताते हुए ‘रामचरितम्’ का उद्धरण दिया है
सुराप्रतिग्रहाद् देवा: सुरा इत्यभिविश्रुता:.
अर्थात: सुरा ग्रहण करते रहने के कारण देवता ‘सुर’ नाम से प्रसिद्ध हुए।
सोमरस और सुरा में फर्क है– ऋग्वेद में शराब की घोर निंदा करते हुए कहा गया है-
हृत्सु पीतासो युध्यन्ते दुर्मदासो न सुरायाम्।।
अर्थात: सुरापान करने या नशीले पदार्थों को पीने वाले अक्सर युद्ध, मार-पिटाई या उत्पात मचाया करते हैं।
सुरा कैसे सोमरस से अलग है… सुरा बनाने की विधि
यजुर्वेद के एक मन्त्र में सुराकार अर्थात्सुरा बनाने वाले की ओर सङ्केत किया गया है – कीलालाय सुराकारम् । इस मन्त्र का कथन है कि सुराबनाने वाला सुराकार है। यजुर्वेद के अन्य मन्त्रों में सुरा निर्माण की प्रक्रिया का भी वर्णन किया गया है-
शष्पाणि… तोक्मानि… सोमस्य लाजा.
सोमांशवो मधु।
मासरं… नग्नहुः । रूपमेतद् उपसदाम्
एतत् तिस्त्रो रात्री: सुराऽऽसुता।
अर्थात: इन मन्त्रों में कहा गया है कि अङ्कुरित चाँवल, अङ्कुरित जौ और खील का चूरा, सोमरस में डालकर तीन रात तक रखने से सुरा तैयार हो जाती है।
वेदों में दी गई इन ऋचाओं में सोमरस का विस्तृत वर्णन किया गया है… ऋग्वेद की एक ऋचा में लिखा गया है कि ‘यह निचोड़ा हुआ शुद्ध दधिमिश्रित सोमरस, सोमपान की प्रबल इच्छा रखने वाले इन्द्रदेव को प्राप्त हो।। (ऋग्वेद-1/5/5) …हे वायुदेव! यह निचोड़ा हुआ सोमरस तीखा होने के कारण दुग्ध में मिश्रित करके तैयार किया गया है। आइए और इसका पान कीजिए।। (ऋग्वेद-1/23/1)
शतं वा य: शुचीनां सहस्रं वा समाशिराम्। एदुनिम्नं न रीयते।। (ऋग्वेद-1/30/2)
अर्थात: नीचे की ओर बहते हुए जल के समान प्रवाहित होते सैकड़ों घड़े सोमरस में मिले हुए हजारों घड़े दुग्ध मिल करके इन्द्रदेव को प्राप्त हों।
इन सभी मंत्रों में सोम में दही और दूध को मिलाने की बात कही गई है, जबकि यह सभी जानते हैं कि शराब में दूध और दही नहीं मिलाया जा सकता। भांग में दूध तो मिलाया जा सकता है लेकिन दही नहीं, लेकिन यहां यह एक ऐसे पदार्थ का वर्णन किया जा रहा है जिसमें दही भी मिलाया जा सकता है। अत: यह बात का स्पष्ट हो जाती है कि सोमरस जो भी हो लेकिन वह शराब या भांग तो कतई नहीं थी और जिससे नशा भी नहीं होता था अर्थात वह हानिकारक वस्तु तो नहीं थी। देवताओं के लिए समर्पण का यह मुख्य पदार्थ था और अनेक यज्ञों में इसका बहुविध उपयोग होता था। सबसे अधिक सोमरस पीने वाले इन्द्र और वायु हैं। पूषा आदि को भी यदा-कदा सोम अर्पित किया जाता है, जैसे वर्तमान में पंचामृत अर्पण किया जाता है।
ऋग्वेद में रस शब्द का प्रयोग कभी मधु, कभी गौ-क्षीर, कभी सोमरस अथवा कभी रस युक्तता को प्रकट करनेके लिए हुआ है ।
ऋग्वेद के मन्त्रों में द्यावापृथिवी में हाइड्रोजन की उपस्थिति सोम के रूप में कही गयी है –
यं सोममिन्द्र पृथिवीद्यावा गर्भं न माता बिभृतस्त्वाया।
धृतेन द्यावापृथिवी अभीवृते धृतश्रिया धृतपचा धृतावधा।
अर्थात: उपर्युक्त मन्त्रों में हाइड्रोजन की उपस्थिति पृथिवी और आकाश में सर्वत्र बताते हुए हाइड्रोजन को ही द्यावापृथिवी में वृद्धि, विस्तार और प्रकाश का कारण कहा है साथ ही मन्त्र में यह भी कहा गया है किसोम को द्यावापृथिवी ने गर्भस्थ बालक की तरह अपने अन्दर धारण किया हुआ है।
ऋग्वेद के एक मन्त्र का कथन है कि सोम देवों का पेय पदार्थ है –
अश्नवत् सोमसुत्वा।
अर्थात: सोम का अर्क निकालने की प्रक्रिया को सोम सुति और सोमसुत्या कहते थे और इस प्रकिया सेरस निकालने वाले सोमसुत् और सोमसुत्वन् कहलाते हैं। इस कार्य को पवित्र माना गया है। ऋग्वेद कापूर्ण नवम् मण्डल (११०८ मन्त्र) सोम के विषय में हैं। द्राक्षासव के समान ही सोम का भी आसव तैयारकिया जाता था जिसे देवता पेय पदार्थ के रूप में ग्रहण करते थे।
ऋग्वेद में कहा गया है कि जल में सोम आदि रसों को मिलाकर सेवन करने से मनुष्य दीर्घायु होता है-
यद् देवा अदः सलिले, सुसंरब्धा अतिष्ठत।‘
मन्त्र में कहा गया है कि जल में हमेशा देव तैयार होते हैं तथा जल में कोई भी कभी भी इच्छानुसार परीक्षण कर सकता है
इस मन्त्र का कथन है कि सोम के मिश्रण से तीन प्रकार के पेय बनाये जाते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से त्र्याशिर: कहते हैं।
सोमा इव त्र्याशिरः।
दही के मिश्रण से बना पेय दध्याशिर्, सत्तू के मिश्रण से बना पेय यवाशिर् एवं दूधआदि के मिश्रण से बना पेय गवाशिर् कहलाता है। ऋग्वेद के एक मन्त्र में मध्वो रसम् कहकर मधुरसायन का भी वर्णन किया गया है। इसमें सोम के तुल्य ही मधु (शहद) का आसव और रसायन तैयारकिये जाने का वर्णन है
एक मन्त्र में सुरा निर्माण करने वाले को सुरावत् कहा गया है। ऋग्वेद के ही एक अन्य मन्त्र मेंसुरा रखने के पात्र, पीने के पात्र एवं उससे उत्पन्न होने वाली बीमारी का सङ्केत किया गया है। इस मन्त्र मेंसुरा रखने के पात्र को सुराधान, सुरा पीने के पात्र को सुराकंस एवं सुरा से उत्पन्न होने वाली बीमारी कोसुराम कहा गया है।
सुरा को समझने के लिए इन दो शब्दों ‘सौत्रामणी’ और ‘किण्वीकरण‘ को समझना होगा-
- सौत्रामणी यज्ञ क्या है जिसमें सुरा का प्रयोग होता था- सौत्रामणि = सु त्रमण = अर्थात उत्तम प्रकार से रक्षा करना। तैत्तरीय संहिता में इन्द्र कि बिखरी हुई शक्तियों को एकत्रित करने के लिए सौत्रामणि यज्ञ का वर्णन है।
- सुरा में ‘किण्वीकरण‘ होना आवश्यक- सोम और सुरा में एक मुख्य अंतर यह भी है कि सोमरस सोमलता को कूटकर निकाला हुआ रस है। जबकि सुरा में ‘किण्वीकरण’ होना आवश्यक है। किण्वीकरण एक विधि है इसके द्वारा किसी भी शक्करमय पदार्थ या स्टार्चमय पदार्थ से ऐल्कोहल व्यापारिक मात्रा में बनाई जाती है। इस अभिक्रिया को आज की साइंटिफिक भाषा में लिखा जा सकता है- C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2
सौत्रामणि यज्ञ- इन्द्र के निमित्त जो यज्ञ किया जाता है, उसे सौत्रामणि यज्ञ कहते हैं। वह दो प्रकार का होता है- प्रथम स्वतन्त्र और द्वितीय अंगभूत। स्वतन्त्र भूत केवल ब्राह्मणों के लिये विधेय है और अँगभूत, क्षत्रिय और वैश्यों के लिये।
- इस यज्ञ के दो भेद हैं – 1- कौकिली 2- चरक सौत्रामणि। कौकिली सौत्रामणि में साम मन्त्रों का गायन किया जाता है। चरक सौत्रामणि साधारण सौत्रामणि है जिसका सम्पादन प्रायः राजसूय यज्ञ के एक माह बाद किया जाता है। इस यज्ञ में तीन दिनों तक भिन्न-भिन्न प्रकार की सुरा बनाई जाती है। आजकल सुरा कीजगह दूध का प्रयोग किया जाता है।
- तैत्तिरीय संहिता (2.5.1) तथा शतपथ ब्रह्माण (1.6.3, 5.5.4) में त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप की गाथा आयी है। विश्वरूप के तीन सिर थे, एक से वह सोम पीता था, दूसरे से सुरा और तीसरे से भोजन करता था। इन्द्र में विश्वरूप के सिर काट डाले, इस पर त्वष्टा बहुत क्रोधित हुआ और उसने सोमयज्ञ किया जिसमें इन्द्र को आमन्त्रित नहीं किया। इन्द्र ने बिना निमन्त्रित हुए सारा सोम पी लिया। इतना पीने से इन्द्र को महान कष्ट हुआ, अत: देवताओं ने सौत्रामणी नामक इष्टि द्वारा उसे अच्छा किया। सौत्रामणि यज्ञ उस पुरोहित के लिए भी किया जाता था जो अधिक सोम पी जाता था। इससे मदमत्त व्यक्ति वरम या विरेचन करता था। (देखिए कात्यायन श्रौतसूत्र 19.1.14) शतपथ ब्राह्मण (12.7.3.5) एवं कात्यायन श्रौतसूत्र (191.20-27) में सुरा बनाने की विधि बतायी गयी है। जैमिनि (3.5.14-15) में सौत्रामणी यज्ञ के विषय में चर्चा है। इस यज्ञ में कोई ब्राह्मण बुलाया जाता था और उसे सुरा का तलछट पीना पड़ता था।
सुरा के प्रकार
बौधायन ग्रन्थ में सुरा के अलावा वारूणी और शीघ्र का भी वर्णन है।
पचित्तिय में पिठ-सुरा, पूव-सुरा, ओदन सुरा (किण्वयाकिखत्ता संभारसंयुत्ता) तथा मैरेय का उल्लेख है।
कौटिल्य ने बेदक, प्रसन्ना, आसव, अरिष्ठ, मरैय व मधु के अलावा कापिशायन और हारहूरक आदि मद्य का वर्णन है।
रामायण में भी मैरेय, सुरा और वारूणी का उल्लेख है। शर्करासव, माध्वीक, पुष्पासव और फलासवका भी रामायण में वर्णन है।
चरक ने सुरा, मदिरा, अरिष्ट, शार्कर, गौड़, मद्य, मधु आदि को मद्यपेय माना है।
सुश्रुत सूत्र में सामान्य सुरा, श्वेतसुरा यवसुरा, शीधु, नरैया और आसव का वर्णन है।
वाणभट्ट ने सुरा वारूणी, अरिष्ट, मार्दीक, खार्जूर, शर्करा, शीधु, आसव, मध्वासव आदि मद्यों का वर्णन है।
कालीदास ने नारिकेलासव, शीधु, पुष्पासव, मधु, द्राक्षासव, वारूणी व हाला आदि मद्य बताया है।
मादक पेय के रूप में ‘सुरा‘ और ‘मैरेय‘ के उल्लेख मिलते हैं- जातकों में मधुशाला के वर्णन उपलब्ध होते हैं। महावग्ग में मज्जा का उल्लेख है। यह एक प्रकार की सुरा थी जिसका प्रयोग औषधि के रूप में होता था। जातकों से ज्ञात होता है कि लोग उत्सव के दिन जी भरकर खाते पीते और आनन्द मनाते थे जिसमें मद्यपान का प्रमुख स्थान रहताथा। इनमें एक उत्सव का नाम ही सुरानक्षत्र पड़ गया, अनियन्त्रित सुरापान, नृत्य, संगीत और भोजन इसकी प्रमुख विशेषताएँ थी। विनयपिटक के अनुसार श्रमण तथा भिक्षु के लिए सुरापान वर्जित था।
वैदिक काल में मद्यपान का प्रचलन
सोम का प्रयोग केवल देवगण एवं पुरोहित लोग कर सकते थे, किन्तु सुरा का प्रयोग अन्य कोई भी कर सकता था, और वह बहुधा देवगणों को समर्पित नहीं होती थी।
सोम के अलावा 13 प्रकार के अन्य मद्यों का उल्लेख आता है- सुरा, हलिप्रिया, हाला, परिसुत, वरूणात्मजा, गन्धोत्तमा, प्रसन्ना, इरा, कादम्बरी, परिसुता, मदिरा, कश्यम् और मद्यम।
मद्य पान का उल्लेख
- मदिरा पान के समय खाने वाले नमकीन का ‘नाम अवदश बताए गया है।
- मदिरा पीने की अवसर के भी दो नाम बताए गये हैं – मधुवार, मधुक्रम।
- महुए की शराब के चार नाम बताए गए हैं- मध्वासन, माधवक, मधु, मार्दीकम।
- ईख से निर्मित शराब के तीन नाम- मेरेयम, आसव एवं शीधु बताए गए हैं।
- मदिरा निर्माण के दो नाम- सन्धानम् एवं अभिषव बताए गए हैं।
- मदिरा पीने के स्थानों के नाम शुण्डा, पानम्, मदस्थानम्, आपानम्पान गोष्ठिका बताए गए हैं।
- मदिरा के काढ़े के लिए पिसे हुए पदार्थ का नाम मेदक, जगल बताए गया है।
- मदिरा पीने के चषक के दो नाम – चषक एवं पानपात्रम् बताए गए हैं।
- शराब पीने या परोसने का नाम सरक अनुतर्षणम् बताया गया है।
याज्ञवल्क्य में रंगरेज, वधिक, रजक, बंदीजन, मद्य बेचने वाले कुलाल, तेलीया गाड़ीवान के घर अन्न ग्रहण करने का निषेध है।
भागवतमहापुराण (स्कन्ध 8, अध्याय 5) के अनुसार चाक्षुष-मन्वन्तर (पौराणिक कालगणनानुसार लगभग 42.89 करोड़ वर्ष पूर्व) भगवान् विष्णु का कच्छप-अवतार हुआ एवं क्षीरसागर के मन्थन से 14 रत्नों में से नौवे क्रम में निकली सुरा लिए हुए वारुणी देवी। भगवान की अनुमति के बाद वारुणी देवी ने सुरा को असुरों को सौंप दिया गया।
ऋग्वेद (7.86.6) में वसिष्ठ ऋषि ने वरिण से प्रार्थना भरे शब्दों में कहा है कि मनुष्य स्वयं अपनी वृत्ति या शक्ति से पाप नहीं करता, प्रत्युत भाग्य, सुरा, क्रोध जुआ एंव असावधानी के कारण वह ऐसा करता है। सोम एवं सुरा के विषय में अन्य संकेत देखिए ऋग्वेद (8.2.12, 1.116.7, 1.191.10, 10.107.9, 10.13.4 एंव 5)।
अथर्ववेद (4.34.6) में ऐसा आया है कि यज्ञ करने वाले को स्वर्ग में घृत एवं मधु की झीलें एवं जल की भांति बहती हुई सुरा मिलती है। ऋग्वेद (10.131.4) में सोम-मिश्रित सुरा को सुराम कहते हैं और इसका प्रयोग इन्द्र ने असुर नमुचि के युद्ध में किया था। अथर्ववेद में सुरा का वर्णन कई स्थानों पर हुआ है, यथा 14.1.35-36, 15.9.2-3। वाजसनेयी संहिता (19.7) में भी सुरा एंव सोम का अन्तर स्पष्ट किया गया है।
शतपथ ब्राह्मण (5.5.4.28) में सोम को ‘सत्य, समृद्धि एंव प्रकाश’ तथा सुरा को ‘असत्य, क्लेश एंव अंधकार’ कहा है। इसी ब्राह्मण (5.5.4.21) ने सोम और सुरा के मिश्रण के भयानक रुप का वर्णन किया है।
काठकसंहिता (12.12) में मनोरंजक वर्णन आया है; प्रौढ़, युवक, वधुएं और श्वशुर सुरा पीते हैं, साथ-साथ प्रलाप करते हैं; मूखर्ता (विचारहीनता) सचमुच अपराध है। इसलिए ब्राह्मण यह सोचकर कि यदि मैं पीऊंगा तो अपराध करूंगा, सुरा नहीं पीता, अत: यह क्षत्रिय के लिए है; ब्राह्मण से कहना चाहिए- यदि क्षत्रिय सुरा पीये तो उसकी हानि नहीं होगी”। इस कथन से स्पष्ट है कि काठकसहिंता के काल में सामान्यत: ब्राह्मण लोग सुरा पीना छोड़ चुके थे। सौत्रामणी यज्ञ में सुरा का तलछट पीने के लिए भी ब्राह्मण का मिलना कठिन हो गया था।
तैत्तिरीय ब्राह्मण 1.8.6) ऐतरेय ब्राह्मण (37.4) में अभिषेक के समय पुरोहित द्वारा राजा के हाथ में सुरापात्र का रखा जाना वर्णित है। छान्दोग्योपनिषद् (5.10.9) में सुरापान करने वाले को पांच पापियों में परिगणित किया गया है। इसी उपनिषद् (5.11.5) में केकय के राजा अश्वपति ने कहा है कि उसके राज्य में मद्यप नहीं पाये जाते।
कुछ गृह्यसूत्रों में एक विचित्र बात पायी जाती है- अन्वष्टका के दिन जब पुरुष पितरों को पिण्ड दिया जाता है तो माता, पितामही (दादी) एवं प्रपितामही को पिण्डमान के साथ सुरा भी दी जाती है। उदाहरणार्थ, आश्व- लायनगृह्यसूत्रों (2.5.5) में आया है- “पितरों की पत्नियों को सुरा दी जाती है और पके हुए चावल का अवशेष भी”। यही बात पारस्करगृह्यसूत्रों (3.3) में भी पायी जाती है।
काठकगृह्यसूत्र (65.7-8) में आया है कि अन्वष्टका में नारी पितरों के पिण्डों पर चमस से सुरा छिड़की जानी चाहिए और वे पिण्ड नौकरों या निषादों द्वारा खाए जाने चाहिए, या उन्हें पानी या अग्नि में फेंक देना चाहिए या ब्राह्मणों को खाने के लिए दे देना चाहिए। इस विचित्र बात का कारण बताना कठिन है। यदि अंदाजा लगाए तो कहा जा सकता है कि (1) उन दिनों नारियां सुरापान किया करती थीं (सम्भवत: लुक-छिपकर), या (2) गृह्यसूत्रों के काल में अंतर्जातीय विवाह चलते थे और घर में क्षत्रिय और वैश्य पत्नियां सुरापान किया करती थीं।
मनु (11.15) ने ब्राह्मणों के लिए सुरापान वर्जित माना है, किन्तु कुल्लूक का कथन है कि कुछ टीकाकारों के मत से यह प्रतिबन्ध नारियों पर लागू नहीं होता था। गृह्यसूत्रों की दृष्टि में उपर्युक्त छूट के लिए जो भी कारण रहे हों, किन्तु यह बात काठकसंहिता एंव ब्राह्मण ग्रन्थों के लिए ही नहीं प्रत्युत अकमत से धर्मसूत्रों एंव स्मृतियों के लिए पूर्णरूपेण अमान्य रही है।
गौतम (2.25), आपस्तम्बधर्मसूत्र (1.5.17.21), मनु (11.14) ने एक स्वर से ब्राह्मणों के लिए सभी अवस्थाओं में सभी प्रकार की नशीली वस्तुओं को वर्जित जाना है। सुरा या मद्य का पान एक महापातक कहा गया है (आपस्तम्बधर्मसूत्र 1.7.21.8, वसिष्ठधर्मसूत्र 1.20, विष्णुधर्मसूत्र 15.1, मनु 11.54, याज्ञवल्क्य 3.227)। यह सब होते हुए भी बौधायनधर्मसूत्र (1.2.4) ने लिखा है कि उत्तर के ब्राह्मणों के व्यवहार में लायी जाने वाली विचित्र पांच वस्तुओं में सीधु (आसब) भी है। इस धर्मसूत्र ने उन सभी विलक्षण पांचों वस्तुओं की भर्त्सना की है।
मनु (11.13-14) की ये बातें निबन्धों एंव टीकाकारों ने उद्धत की हैं- “सुरा भोजन का मल है, और पाप को मल कहते हैं, अंत: ब्राह्मणों, राजन्यों (क्षत्रियों) एंव वैश्यों को चाहिए कि वे सुरा का पान न करें। सुरा तीन प्रकार की होती है- गुड़ वाली, आटे वाली तथा मधूक (महुआ) के फूलों वाली (गौड़ी, पैष्टी एंव माध्वी), इनमें किसी को भी ब्राह्मण ने पीये”।
महाभारत (उद्योगपर्व 55.5) में वासुदेव एवं अर्जुन मदिरा (सुरा) पीकर मत्त हुए कह गये हैं। यह मदिरा मधु से बनी थी। तन्त्रवार्तिक (पृ. 209-210) ने लिखा है कि क्षत्रियों को यह वर्जित नहीं थी अत: वासुदेव एवं अर्जुन क्षत्रिय होने के नाते पापी नहीं हुए।
मनु (11.93-94) एवं गौतम (2.25) ने ब्राह्मणों के लिए सभी प्रकार की सुरा वर्जित मानी है, किन्तु क्षत्रियों एवं वैश्यों के लिए केवल पैष्टी वर्जित है। शूद्रों के लिए मद्यपान वर्जित नहीं था, यद्यपि वृद्ध हारीत (9.277-278) ने लिखा है कि कुछ लोगों के मत से सत्-शूद्रों को सुरापान नहीं करना चाहिए। मनु की बात करते हुए वृद्ध हारीत ने कहा है कि झूठ बोलने, मांस- भक्षण करने, मद्यपान करने, चोरी करने या दूसरे की पत्नी चुराने से शूद्र भी पतित हो जाता है। प्रत्येक वर्ण के ब्रह्मचारी को सुरापान से दूर रहना पड़ता था- (आपस्तम्बधर्मसूत्र 1.1.2.23, मनु 2.177 एवं याज्ञवल्क्य 1.33)।
महाभारत (आदिपर्व 76.77) ने शुक्र, उनकी पुत्री देवयानी एवं शिष्य कच की गाथा कही है और लिखा है कि शुक्र ने सबसे पहले ब्राह्मणों के लिए सुरापान वर्जित माना और व्यवस्था दी जी उसके उपरान्त सुरापान करने वाला ब्राह्मण ब्रह्महत्या का अपराधी माना जायेगा। मौशलपर्व (1.29-30) में आया है कि बलराम ने उस दिन से जब कि यादवों के सर्वनाश के लिए मूसल उत्पन्न किया गया, सुरापान वर्जित कर दिया और आज्ञा दी कि अनुशासन का पालन न करने से लोग सूली पर चढ़ा दिए जाएंगे।
शान्तिपर्व (34.20) ने यह भी लिखा है कि यदि कोई भय या अज्ञान से सुरापान करता है तो उसे पुन: उपनयन करना चाहिए। विष्णुधर्मसूत्र (22.83-84) के अनुसार ब्राह्मणों के लिए वर्जित मद्य 10 प्रकार की हैं- माधूक (महुआ वाली) , ऐक्षव (ईख वाली), टांक (टंक या कपित्थ फल वाली) कौल (कोल या बदर या उन्नाव नामक बेर वाली), खार्जूर (खजूर वाली), पानस (कटहर वाली) अंगूर, माध्वी (मधु वाली), मैरेय (एक पौधे के फूलों वाली) एवं नारिकेलज (नारिकेल वाली) किन्तु ये दसों क्षत्रियों एवं वैश्यों के लिए वर्जित नहीं है। सुरा नामक मदिरा चावल के आटे से बनती थी।
मनु (9.80) एवं याज्ञवल्क्य (1.73) के मतानुसार मद्यपान करन वाली पत्नी (चाहे वह शूद्र ही क्यों न हो और ब्राह्मण को ही क्यों न ब्याही गयी हो) त्याज्य है। मिताक्षरा ने उपर्युक्त याज्ञवल्क्य के कथन की टीका में पराशर (10.26) एंव वसिष्ठधर्मसूत्र का हवाला देते हुए कहा है कि मद्यपान करने वाली स्त्री के पति का अर्ध शरीर बड़े भारी पाप का भागी होता है।
धर्मसूत्रों में मद्य के प्रकार
गौतम धर्मसूत्र में सुरा का ही वर्णन मिलता है। आपस्तम्ब (प्रमुख धर्मसूत्रों एवं स्मृतियों में प्रायश्चित विधान- शिखा शर्मा) ने भी सुरा शब्द का ही प्रयोग किया है। आपस्तम्ब धर्मसूत्र के अनुसार सुरापान करने वाला व्यक्ति अग्नि पर खौलाई गयी सुरा पिये। बौधायन (बौधायन धर्मसुत्र) ने सुरा के अलावा वारूणी और शीघ्र का भी वर्णन किया है।
ऋग्वेद के वर्णन से लगता है कि मधु भी मादक पेय था, मधु का प्रयोग रस के संदर्भ में किया गया है। ऋग्वेद के एक श्लोक “स्वादु रसो मधुपेयो वराय” (6.44.21) में इससे राजा के मस्त होने का उल्लेख है।
बौद्ध साहित्य संयुक्त निकाय में सुरा और मैरेय का वर्णन मिलता है। धम्मपद में भी इन्हीं का वर्णन मिलता है। धम्मपद , 22/4,5(5) सुरा – मैरेय – मद्य – विरमणम् – “बौद्धभिक्षवे गृहस्थाय च सुरापानम् , मद्यपानम् , मादक वस्तु सेवनं च वर्जितमस्ति”। महावग्ग (89-223) में मज्जा का उल्लेख है। यह एक प्रकार की सुरा थी जिसका प्रयोग औषधि के रूप में होता था।
पाचित्तिय (भाग-6) में सुरा के अनेक प्रकारों का वर्णन मिलता है- मैरेय एक प्रकार की सुरा है जिसे फूलों के आसव से बनाया जाता था। इसके भी कई प्रकारों का वर्णन मिलता है जैसे – पुष्पों से बना पुष्पासव, फलों से बना फलासव और मधु से बना मध्वासव। पाचवें उपदेश में सूरा, मैरेय और मज्जा (मद्य) के सेवन पर प्रतिबंध की बात की गई है। कई और सुरा का वर्णन भी मिलता है- पिठ-सुरा, पूव-सुरा, ओदन सुरा, जो किण्वयक्खित्ता यानी फर्मेंटेशन के जरिए बनाई जाती थी।
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र (अध्यायः25, 02.25.16) में मद्य के कई प्रकारों का वर्णन किया है – मेदक, प्रसन्ना,आसव, अरिष्ट, मैरेय और मधु। कौटिल्य ने कापिशायन और हारहूरक नामक मद्य का भी वर्णन किया है। सुरा के प्रकारों का वर्णन करते हुए कौटिल्य ने इसके चार प्रकार बताये हैं –सहकारसुरा, रसोत्तरा,बीजोत्तरा और सम्भारिका।
रामायण (बालकाण्ड- 1/45-23&25) में मद्य निम्न प्रकार मैरेय, सुरा और वारूणी का वर्णन मिलता है। वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनन्दन।। उत्पपात महाभागा मार्गमाणा परिग्रहम्। दितेः पुत्रा न तां राम जगृहुवरुणात्मजाम्।। अदितेस्तु सुता वीर जगृहुस्तामनिन्दिताम् ।असुरास्तेन दैतेयाः सुरास्तेनादितेः सुताः।। इसके अलावा शर्करासव, माध्वीक, पुष्पासव और फलासव का भी वर्णन मिलता है।
रामायण (सुंदरकाण्ड- 5/11–20) में रावण की पानशाला के बारे में कहा गया है- दिव्याः प्रसन्ना विविधाः सुराः कृत सुरा अपि। शर्कर आसव माध्वीकाः पुष्प आसव फल आसवाः। वास चूर्णैः च विविधैर् मृष्टाः तैः तैः पृथक् पृथक्।। सदैव मधु-आसव (5/11/23), शर्करासव (2/94/24), पुष्पासव (5/11/23), फलासव(5/11/23), से भरी रहती थी। रामायण में रावण के रनिवास में स्थित पानशाला का विशद वर्णन हैं।
महाभारत काल में अधिकतर सुरा का ही प्रचलन था। परन्तु माध्वीक, कैलावत आदि का भी वर्णन मिलता है। कर्णपर्व- अध्याय:61- सतन्यस्य मातुर मधुसर्पिषॊ वा; माध्वीक पानस्य च सत्कृतस्य। स्त्रीपर्व- अध्याय:20- लज्ज माना पुरैवैनं माध्वीक मदमूर्छिता।
मनु ने मद्य के निम्न प्रकार वारुणी, सुरा और आसव का वर्णन किया है तथा सुरा अधिक बल दिया गया है। मनुस्मृति के श्लोक 11/95 ‘‘यक्षरक्षः पिशाचान्नं मद्यं मांस सुरा ऽऽ सवम्। सद् ब्राह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्नता हविः।” में कहा गया है कि ‘‘मद्य, मांस, सुरा और आसव ये चारों यक्ष, राक्षसों तथा पिशाचों के अन्न (भक्ष्य पदार्थ) हैं, अतएव देवताओं के हविष्य खाने वाले ब्राह्मणों को उनका भोजन (पान) नहीं करना चाहिये।”
हरिवंश पुराण (विष्णु पर्व अध्याय 89 श्लोक 36-52) में मैरेय, माध्वीक, सुरा और आसव नाम मधु से भरे हुए कलश का उल्लेख है।
चरक (चरक संहिता, सूत्रस्थान- 27.180) ने निम्न प्रकार के मद्यों का वर्णन किया है – “हिक्काश्वासप्रतिश्यायकासवर्षोंग्रहारुचौं। वम्यानाह विबन्धेषु वातघ्नी मदिरा हिता।।“ आचार्य चरक ने मद्य को अनेक नाम यथा- मदिरा, जगल, अरिष्ट, शार्कर, धातकी (धाय के फूलों से निर्मित)मधुमद्य, सुरा, जौ की सुरा, तुषोदक अम्लकजिक, मैरेय, हाला, आदि से उल्लेख किया है। स्वभाव से सभी प्रकार केमद्य रस में अम्ल उष्णवीर्य आदि विपाक में भी अम्ल होते हैं मदिरा पीने से होने वाले लाभ का भी वर्णन किया है।
सुश्रुत (सुश्रुत संहिता- 174-206) ने भी मद्य के निम्न प्रकारों कावर्णन किया है – द्राक्षा मद्य, खार्जूर, प्रसन्ना, सुरा, इसके कई प्रकार है – सामान्य सुरा, श्वेतसुरा, यवसुरा,शीध्रु, मैरेय और आसव आदि।
वाणभट्ट ने निम्न प्रकार के मद्यों का वर्णन किया है सुरा, वारूणी, अरिष्ट, मार्दीक.खार्जूर, शार्केरा, शीधु, आसव, मध्वासव आदि ।
कालिदास की रचनाओं में मद्य के नारिकेलासव, शीधु, पुष्पासव, मधु, द्राक्षासव, वारूणीऔर हाला आदि प्रकारों का वर्णन मिलता है।’ कालिदास की रचनाओं में मघ के लिये मद्य आसव’ ‘मधामदिरा, कादम्बरी’ आदि पदों का प्रयोग हुआ है। कालिदास विशेषकर मद्य के तीन प्रकारों का उल्लेख करते हैं नारियल से बना हुआ नारिकेलासव, गन्ने के रस से बना हुआ शीघु और पुष्पों से निकाला हुआ पुष्पासव’। बहुधा धनिक वर्ग के लोग सुगंधित मद्य का ही प्रयोग करते थे। मृच्छकटिक में मदिरापान एवं मदिरालय के उल्लेख मिलते हैं।
चतुर्भाणी में आये धूर्तविट संवाद से लगता है कि शराब को सुगन्धित और रूचिकर बनाने के लिए उसमें कमल की पंखड़ियां तथा सहकार तैल डाला जाता था।
सुबन्धु के “वासवदत्ता” में निम्न प्रकार के मद्यों का वर्णन मिलता है यथा – मधु,वारूणी और सुरा ।
बाण के “हर्षचरित’ में कई प्रकार के मद्यों का वर्णन मिलता है – सोम, मधु,मदिरा, प्रसन्ना, सुरा, सीधु, वारूणी और आसव आदि ।
मद्यनिषेध- सुरा-त्याग
उपरोक्त संदर्भों से साफ है कि अलग अलग काल में मद्य का प्रचलन था। लेकिन इसका सेवन सीमित था। ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर सुरा-त्याग का उल्लेख किया गया है। मदिरा पान को पाप की ओर प्रवृत्ति तक कहा गया है।
ऋग्वेद (7.86.6) और अथर्ववेद (6.70.1; 14.1.35-36) में स्पष्ट उल्लेख है कि वैदिक युग में आरम्भिक काल से लोग सुरा के गुणों और अवगुणों से परिचित थे। वैदिक साहित्य में स्थान-स्थान पर सुरा की भरपूर निन्दा की गई है। मांस और जुआ के समकक्ष ही इसे बुरा माना गया है।
ऋग्वेद (8.2.12; 8.21.14) में कहा गया है कि मनोरंजन के लिए जो सभायें जुटती थीं, उनमें मदिरा पान करने वाले लोग लड़-झगड़ पड़ते थे। ऋग्वेद (10.131.5) के मुताबिक अधिक मदिरा पान करने वाले लोग सुराग रोग से पीड़ित होते थे। मदिरा पान से पाप की ओर प्रवृत्ति होती थी।
ऋग्वेद (7.86.6) शतपथ ब्राह्मण (5.1.5.28) के अनुसार सुरा का वैदिक काल से ही ऋषियों ने कभी आदर का स्थान नहीं दिया, क्योंकि इसके पीने से मानव की असत्प्रवृत्तियों को उत्तेजना मिलती है।
रघुवंश (4.42), कुमारसंभव (6.42), नैषधीयचरित (16.98) के अनुसार उपनिषद् युग में किसी राजा के लिए गौरव की बात थी कि उसके राज्य में एक भी सुरापायी न था। मदिरापान पांच महापातकों में गिना गया है। मनु ने तो ब्राह्मण, क्षत्रियऔर वैश्य किसी के लिए भी मदिरा पान उचित नहीं माना।
महाभारत, शान्तिपर्व (111.29)- महाभारत के अनुसार सुरा का सिद्धान्त रूप में निषेध किया गया, यद्यपि स्थान-स्थान पर सुरा पीने वालों का उल्लेख मिलता है। मधु, मांस और मद्य का परित्याग करने वाला सभी कठिनाइयों को पार कर जाता है। यदि औषधि रूप में अथवाभूल से भी मद्य पी लिया तो पुन: उपनयन करना पड़ता था
महर्षि वाल्मीकि ने रामायण (4.33.46) में लिखा है कि धर्म और अर्थ की सिद्धि के लिए मदिरा पान हानिकारक है। मदिरा पान करने में धर्म, अर्थ और काम सभी नष्ट हो जाते है। जो ब्राह्मण सुरापायी होते थे, उन्हें सड़कों पर लोग धिक्कारते चलते थे।
विष्णुपुराण (2.6-9) में विहित है कि मदिरापान करने वाले तथा ऐसे व्यक्ति के साथ सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति नरक में जाते हैं। कतिपय उद्धरणों में मदिरा बनाने वाले व्यक्ति को भी निन्द्य बताया गया है।
वायु पुराण (18.33) और ब्रह्माण्ड पुराण (2.12.133) में निरूपित है कि मदिरा बनाने वाला व्यक्ति पूयवह नामक नरक में जाता है।
ऋग्वेद (7.86.6) में एक स्थल पर मदिरा पानको पाप का कारण बताया गया है।
शतपथ ब्राह्मण (5.1.5.28) “अमृतं पाप्मा तमः सुरा” में सुरा की उपमा असत्य, दुःख और अन्धकार से दी गई है।
मनुस्मृति (9.235) में भी मदिरा पान करने वालों को महापापी की संज्ञा दी गई है।
ब्रह्माण्डपुराण (4.7.78) में वर्णित है कि ब्राह्मण को मोह, स्नेह अथवा इच्छा से मदिरापान नहीं करना चाहिए। एक अन्य स्थल पर वर्णन आता है कि आसवपान केवल क्षत्रिय आदि तीन वर्ण कर सकते हैं। ब्राह्मण की भांति ब्राह्मणी के लिए भी इसे वर्जित किया गया है।
मत्स्य पुराण (25.62) के अनुसार मोहवश मदिरा पान करने वाला ब्राह्मण अधार्मिक है। उसे ब्रह्महत्या का दोष लगता है। लोक तथा परलोकमें उसे गर्हित स्थान मिलता है। इन उद्धरणों से व्यक्त होता है कि ब्राह्मणार्थ मदिरापान आज्ञप्त नहीं था। इस सामान्य नियम के अन्तर्गत क्षत्रियादि तीन वर्ण नहीं आते थे।
विष्णुस्मृति (54.7) में भी मदिरापान करने वाले ब्राह्मण को नारकीय बताया गया है। इसी प्रकार महाभारत ने भी ब्राह्मणार्थ मदिरापान वर्जित किया है। इस सम्बन्ध में महाभारत का उद्धरण बिना किसी अन्तर के मत्स्यपुराण के तद्विषक स्थल के साम्य रखता है।
मदिरापान के दुर्गुणों एवं अव्यवस्थित कृत्यों से राज्यों में प्रतिबंध लगाये जाते रहे हैं। ये प्रतिबंध धार्मिक और सामाजिक आचार के स्वरूप थे। गुजरात में चालुक्य कुमारपाल ने मदिरापा नहीं नहीं बल्कि मदिरा-निर्माणशाला भी बन्द करा दी थी। (मोहराजपराजय, अंक 4, पृ. 83)
हेमचन्द्र के एक विवरण से स्पष्ट है कि चौलुक्य-कुल में मद्यपान वैसा ही वर्जित था, जैसा कि ब्राह्मणों से वर्जित था। (मुनिजिनविजय, राजर्षिकुमार पाल, पृ. 19)
सोमलता
सोम नाम से एक “लता” होती थी- सोम पर्वतों पर उगने वाला पौधा है। यह लता या पौध हिमवन्त से मूजवन्त पर्वत श्रृंखला तक मिलता था। ऋग्वेद के सूक्तों में हिमवन्त (एलबुर्ज पर्वत श्रृंखला, अर्थात ईरान)  तथा मूजवन्त (गान्धार-कम्बोज प्रदेश, अर्थात अफगानिस्तान) पर्वत का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सोम को पर्वतों पर रहने वाला (गिरिष्ठा) तथा अनेक बार पर्वतों पर उगने वाला (पर्वतावृधः) कहा गया है। अथर्ववेद में पर्वतों को सोमन्तो पृष्ठ कहा गया है। ये बातें संकेत करती हैं कि सोमपर्वतों पर उगता था।
तथा मूजवन्त (गान्धार-कम्बोज प्रदेश, अर्थात अफगानिस्तान) पर्वत का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सोम को पर्वतों पर रहने वाला (गिरिष्ठा) तथा अनेक बार पर्वतों पर उगने वाला (पर्वतावृधः) कहा गया है। अथर्ववेद में पर्वतों को सोमन्तो पृष्ठ कहा गया है। ये बातें संकेत करती हैं कि सोमपर्वतों पर उगता था।
इसके अलावा कहां-कहां उल्लेख है- राजस्थान के अर्बुद, उड़ीसा के महेन्द्र गिरी, हिमाचल की पहाड़ियों, विंध्याचल, मलय आदि अनेक पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी लताओं के पाए जाने का उल्लेख भी मिलता है।
यद्यपि सोम को पर्वतों पर उगने वाला एक पौधा कहा गया है फिर भी इसके उत्पत्ति और आवास को स्वर्गीय ही माना गया है। इसके बारे में ऐसी अवधारणा है कि स्वर्ग से इस पौधे को पृथ्वी पर लाया गया है।
ऋग्वेद में इससे सम्बन्धित एक कथा वर्णित है- जिसके अनुसार उत्क्रोश पक्षी द्वाराइस पौधे को स्वर्ग से लाया गया है। कथानुसार उत्क्रोश पक्षी सोम-पौधे के पास उड़ कर गया और इस पौधे के मधुर काण्ड को तोड़ कर, अपने पैरों के बीच दबाकर, तीव्र गति से उड़ता हुआ वज्रधर अर्थात् इन्द्र के लिए सोम लाया।
सोम का रंग– विद्वानों का मत है कि अफगानिस्तान की पहाड़ियों पर पाया जाने वाली यह सोमलता बिना पत्तियों का गहरे बादामी रंग का पौधा है। वहीं जब इससे सोमरस बनाया जाता था तक यह अरूण वर्ण का होता था। ऋग्वेद के एक मन्त्र में इसे अरूण वृक्ष की शाखाभी कहा गया है। कहीं इसके वर्ण के लिए भूरा तथा कहीं हरित शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्राह्ममण ग्रन्थों में सोम लता के अभाव में जिस पौधे को सोमलता का स्थानापन्न किया गया है उसका वर्णभी लाल या अरूण होता था।
ईरान में कुछ वर्ष पहले इफेड्रा नामक पौधे की पहचान कुछ लोग सोम से करते थे– इफेड्रा की छोटी-छोटी टहनियां बर्तनों में दक्षिण-पूर्वी तुर्कमेनिस्तान में तोगोलोक-21 नामक मंदिर परिसर में पाई गई हैं। इन बर्तनों का व्यवहार सोमपान के अनुष्ठान में होता था। यद्यपि इस निर्णायक साक्ष्य के लिए खोज जारी है। हलांकि लोग इसका इस्तेमाल यौन वर्धक दवाई के रूप में करते हैं।
ईरान और आर्यावर्त: माना जाता है कि सोमपान की प्रथा केवल ईरान और भारत के वह इलाके जिन्हें अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहा जाता है यहीं के लोगों में ही प्रचलित थी। इसका मतलब पारसी और वैदिक लोगों में ही इसके रसपान करने का प्रचलन था। इस समूचे इलाके में वैदिक धर्म का पालन करने वाले लोग ही रहते थे। ‘स’ का उच्चारण ‘ह’ में बदल जाने के कारण अवेस्ता में सोम के बदले होम शब्द का प्रयोग होता था और इधर भारत में सोम का।
- कुछ वर्ष पहले ईरान में इंफेड्रा नामक पौधे की पहचान कुछ लोग सोम से करते थे। इफेड्रा की छोटी-छोटी टहनियां बर्तनों में दक्षिण-पूर्वी तुर्कमेनिस्तान में तोगोलोक-21 नामक मंदिर परिसर में पाई गई हैं। इन बर्तनों का व्यवहार सोमपान के अनुष्ठान में होता था। यद्यपि इस निर्णायक साक्ष्य के लिए खोज जारी है।
सोम को 1. स्वर्ग की लता का रस और 2. आकाशीय चन्द्रमा का रस भी माना जाता है... सोम की उत्पत्ति के दो स्थान हैं- ऋग्वेद अनुसार सोम की उत्पत्ति के दो प्रमुख स्थान हैं- 1.स्वर्ग और 2.पार्थिव पर्वत।
वेदों में सोमलता का विशेष महत्व प्रतिपादित किया गया है। ब्राह्मण ग्रन्थों में सोमविषयक अनेक उपाख्यान मिलते हैं। एक उपाख्यान के अनुसार गायत्री नेबाज पक्षी का रूप धारण कर धुलोक से सोम का आहरण किया था। वस्तुतःसोमलता विशेष प्रकार की औषधि है जो पर्वतों पर पायी जाती है। शतपथब्राह्मण इसकी उत्पत्ति की चर्चा करता है। आयुर्वेद में सोमलता को सोमवल्ली,सोमक्षीरी और द्विज प्रिया कहा जाता है। यह सोमलता त्रिदोष – कफ, वात औरपित्त को नष्ट करती है। यह कटु और तिक्त होती है। इसमें रसायन की क्षमता है। इसलिए देवता इसे अधिक चाहते रहे। इसीलिए वेदों में सोम की विशेष प्रशंसा की गयी है। सोम को औषधियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता रहा। इसे औषधियों का राजा कहा गया है।
अग्नि की भांति सोम भी स्वर्ग से पृथ्वी पर आया… ‘मातरिश्वा ने तुम में से एक को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा; गरुत्मान ने दूसरे को मेघशिलाओं से।’ हे सोम, तुम्हारा जन्म उच्च स्थानीय है; तुम स्वर्ग में रहते हो, यद्यपि पृथ्वी तुम्हारा स्वागत करती है। सोम की उत्पत्ति का पार्थिव स्थान मूजवंत पर्वत (गांधार-कम्बोज प्रदेश) है’। -(ऋग्वेद अध्याय सोम मंडल- 4, 5, 6)
- स्वर्गीय सोम की कल्पना चंद्रमा के रूप में की गई है। छांदोग्य उपनिषद में सोम राजा को देवताओं में भोज्य कहा गया है। कौषितकि ब्राह्मण में सोम और चन्द्र के अभेद की व्याख्या इस प्रकार की गई है : ‘दृश्य चन्द्रमा ही सोम है। सोमलता जब लाई जाती है तो चन्द्रमा उसमें प्रवेश करता है। जब कोई सोम खरीदता है तो इस विचार से कि ‘दृश्य चन्द्रमा ही सोम है; उसी का रस पेरा जाए।’
वेदों के अनुसार सोम का संबंध अमरत्व से भी है… वह पितरों से मिलता है और उनको अमर बनाता है। सोम का नैतिक स्वरूप उस समय अधिक निखर जाता है, जब वह वरुण और आदित्य से संयुक्त होता है- ‘हे सोम, तुम राजा वरुण के सनातन विधान हो; तुम्हारा स्वभाव उच्च और गंभीर है; प्रिय मित्र के समान तुम सर्वांग पवित्र हो; तुम अर्यमा के समान वंदनीय हो।’
त्रित प्राचीन देवताओं में से थे। उन्होंने सोम बनाया था तथा इंद्रादि अनेक देवताओं की स्तुतियां समय-समय पर की थीं। महात्मा गौतम के तीन पुत्र थे। तीनों ही मुनि थे। उनके नाम एकत, द्वित और त्रित थे। उन तीनों में सर्वाधिक यश के भागी तथा संभावित मुनि त्रित ही थे। कालांतर में महात्मा गौतम के स्वर्गवास के उपरांत उनके समस्त यजमान तीनों पुत्रों का आदर-सत्कार करने लगे। उन तीनों में से त्रित सबसे अधिक लोकप्रिय हो गए।
कुछ विद्वान इसे ही ‘संजीवनी बूटी’ कहते हैं- सोम को न पहचान पाने की विवशता का वर्णन रामायण में मिलता है। हनुमान दो बार हिमालय जाते हैं, एक बार राम और लक्ष्मण दोनों की मूर्छा पर और एक बार केवल लक्ष्मण की मूर्छा पर, मगर ‘सोम’ की पहचान न होने पर पूरा पर्वत ही उखाड़ लाते हैं। दोनों बार लंका के वैद्य सुषेण ही असली सोम की पहचान कर पाते हैं।
- यदि हम ऋग्वेद के नौवें ‘सोम मंडल’ में वर्णित सोम के गुणों को पढ़ें तो यह संजीवनी बूटी के गुणों से मिलते हैं इससे यह सिद्ध होता है कि सोम ही संजीवनी बूटी रही होगी। ऋग्वेद में सोमरस के बारे में कई जगह वर्णन है। एक जगह पर सोम की इतनी उपलब्धता और प्रचलन दिखाया गया है कि इंसानों के साथ-साथ गायों तक को सोमरस भरपेट खिलाए और पिलाए जाने की बात कही गई है।
सोमरस बनाने की विधि

उच्छिष्टं चम्वोर्भर सोमं पवित्र आ सृज। नि धेहि गोरधि त्वचि।। (ऋग्वेद सूक्त 28 श्लोक 9)
अर्थात : उलूखल और मूसल द्वारा निष्पादित सोम को पात्र से निकालकर पवित्र कुशा के आसन पर रखें और अवशिष्ट को छानने के लिए पवित्र चर्म पर रखें।
औषधि: सोम: सुनोते: पदेनमभिशुण्वन्ति।- निरुक्त शास्त्र (11-2-2)
अर्थात : सोम एक औषधि है जिसको कूट-पीसकर इसका रस निकालते हैं।
- सोम को गाय के दूध में मिलाने पर ‘गवशिरम्’ दही में ‘दध्यशिरम्’ बनता है। शहद अथवा घी के साथ भी मिश्रण किया जाता था। सोम रस बनाने की प्रक्रिया वैदिक यज्ञों में बड़े महत्व की है। इसकी तीन अवस्थाएं हैं- पेरना, छानना और मिलाना। वैदिक साहित्य में इसका विस्तृत और सजीव वर्णन उपलब्ध है।
- सोम के डंठलों को पत्थरों से कूट-पीसकर तथा भेड़ के ऊन की छलनी से छानकर प्राप्त किए जाने वाले सोमरस के लिए इंद्र, अग्नि ही नहीं और भी वैदिक देवता लालायित रहते हैं, तभी तो पूरे विधान से होम (सोम) अनुष्ठान में पुरोहित सबसे पहले इन देवताओं को सोमरस अर्पित करते थे।
- बाद में प्रसाद के तौर पर लेकर खुद भी तृप्त हो जाते थे। आजकल सोमरस की जगह पंचामृत ने ले ली है, जो सोम की प्रतीति-भर है। कुछ परवर्ती प्राचीन धर्मग्रंथों में देवताओं को सोम न अर्पित कर पाने की विवशतास्वरूप वैकल्पिक पदार्थ अर्पित करने की ग्लानि और क्षमा- याचना की सूक्तियां भी हैं।
सोम को दिन में तीन बार सवन अर्थात् दबाया जाता था… सन्ध्याकालीन दबाने के कृत्य को ऋभुओं से’ तथा मध्याहून और प्रातः का सम्बन्ध इन्दरे से किया गया है, किन्तु यज्ञों से प्रसंग में प्राप्त वर्णनों से पता चलता है कि अनेक देव सोम-पान करते थे। सोम यज्ञों के लिए आपस में प्रतिद्वन्द्विता होती थी। इसका वर्णन ऋग्वेद में इस प्रकार किया गया है वसिष्ठ लोग इन्द्र को पाशघुग्न वायत के सोम-यज्ञ से सुदास् के यहां उठा ले आये थे।
सोमरस पीने के फायदे
वैदिक ऋषियों का चमत्कारी आविष्कार- सोमरस एक ऐसा पदार्थ है, जो संजीवनी की तरह कार्य करता है। यह जहां व्यक्ति की जवानी बरकरार रखता है वहीं यह पूर्ण सात्विक, अत्यंत बलवर्धक, आयुवर्धक व भोजन-विष के प्रभाव को नष्ट करने वाली औषधि है।
स्वादुष्किलायं मधुमां उतायम्, तीव्र: किलायं रसवां उतायम।
उतोन्वस्य पपिवांसमिन्द्रम, न कश्चन सहत आहवेषु।।- ऋग्वेद (6-47-1)
अर्थात: सोम बड़ी स्वादिष्ट है, मधुर है, रसीली है। इसका पान करने वाला बलशाली हो जाता है। वह अपराजेय बन जाता है।
शास्त्रों में सोमरस लौकिक अर्थ में एक बलवर्धक पेय माना गया है, परंतु इसका एक पारलौकिक अर्थ भी देखने को मिलता है। साधना की ऊंची अवस्था में व्यक्ति के भीतर एक प्रकार का रस उत्पन्न होता है जिसको केवल ज्ञानीजन ही जान सकते हैं।
सोमं मन्यते पपिवान् यत् संविषन्त्योषधिम्।
सोमं यं ब्रह्माणो विदुर्न तस्याश्नाति कश्चन।। (ऋग्वेद-10-85-3)
अर्थात: बहुत से लोग मानते हैं कि मात्र औषधि रूप में जो लेते हैं, वही सोम है ऐसा नहीं है। एक सोमरस हमारे भीतर भी है, जो अमृतस्वरूप परम तत्व है जिसको खाया-पिया नहीं जाता केवल ज्ञानियों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।
इसके पीने से शरीर एक विचित्र उत्साह से भर जाता था। ऋग्वेद में इसके उल्लासित और कामनीय गुणों का वर्णन करते हुए कल्पना का भी सहारा लियागया है। सोम-पान से इन्द्र के आनन्दोल्लास का कामनीय वर्णन ऋग्वेद के एक समूचे सूक्त (१०.११६) मेंकिया गया है। इस सूक्त में एक जगह उल्लिखित है कि जिस प्रकार वेग से चलने वाले घोड़े रथ को दूरतक खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार ये सोम की घूटें मुझे दूर तक खींच ले जाती है, क्या मैंने सोम का पाननहीं किया है। हन्त! मैं पृथ्वी को यहाँ रखूगा । मैं बड़ों में बड़ा हूँ (महामहः); मैं संसार को नाभि (अन्तरिक्ष)तक उठाये हूँ, क्योंकि मैंने सोम-रस का पान किया है। आर्य भी इसके उल्लासित गुणों से परिचित । प्रगाथ काण्व ऋषि सोम-पान के प्रभाव से आनन्दित होकर कह रहे हैं – “हमने सोम पान किया है, अमरत्व पा लिया है; ज्योर्तिमय स्वर्ग की प्राप्ति कर ली है तथा हमने देवताओं को जान लिया है।’ सामवेदके एक मन्त्र में इसे बुद्धि का विकास करने वाला बताते हुए कहा गया है कि “बुद्धि को बढ़ाने वाला तथास्वयं ज्ञानवान् सोम, सोम-रस निकालने के लिए दो तख्तों के बीच रखा गया। इससे उत्साह और स्फूर्तिदोनों आती थी। सामवेद के एक मन्त्र में इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है – “बल बढ़ाने वाला औरउत्साह बढ़ाने वाला तथा चमकने वाला सोम-रस गाय और वीर पुत्रों की इच्छा करने वालों के द्वारा निचोड़ाजाता है। इसके पीने से सम्भवतः विष का भी प्रभाव समाप्त हो जाता है।
कण्व ऋषियों ने मानवों पर सोम का प्रभाव इस प्रकार बतलाया है- ‘यह शरीर की रक्षा करता है, दुर्घटना से बचाता है, रोग दूर करता है, विपत्तियों को भगाता है, आनंद और आराम देता है, आयु बढ़ाता है और संपत्ति का संवर्द्धन करता है। इसके अलावा यह विद्वेषों से बचाता है, शत्रुओं के क्रोध और द्वेष से रक्षा करता है, उल्लासपूर्ण विचार उत्पन्न करता है, पाप करने वाले को समृद्धि का अनुभव कराता है, देवताओं के क्रोध को शांत करता है और अमर बनाता है’।
सोम विप्रत्व और ऋषित्व का सहायक है। सोम अद्भुत स्फूर्तिदायक, ओजवर्द्धक तथा घावों को पलक झपकते ही भरने की क्षमता वाला है, साथ ही अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति कराने वाला है।
सोमयज्ञ- सोमरस हवन में इस्तमाल होता था
जिन यज्ञों में ‘सोम लता’ से निकाले हुए सोमरस की आहुति प्रदान की जाती है, उन यागों कोसोमयाग कहा जाता है। इसमें सोम नामक लता को कूटकर उसका रस निकालकर उसे हवि के रूप में देवताओं को समर्पित  किया जाता है। “यज्ञं व्याख्यास्यामः”, “स त्रिभिदैविधीयते” श्रौतसूत्रकारों का यहकथन सोमयाग के विषय में ही सिद्ध होता है, क्योंकि यह याग तीनों वेदों की सहायता से सम्पन्न होता है। सोमयज्ञ का हवन करने वाले ऋषियों में कण्व,अंगिरा आदि ऋषि हैं।
किया जाता है। “यज्ञं व्याख्यास्यामः”, “स त्रिभिदैविधीयते” श्रौतसूत्रकारों का यहकथन सोमयाग के विषय में ही सिद्ध होता है, क्योंकि यह याग तीनों वेदों की सहायता से सम्पन्न होता है। सोमयज्ञ का हवन करने वाले ऋषियों में कण्व,अंगिरा आदि ऋषि हैं।
पूर्ववर्णित अग्निहोत्र आदि यज्ञ केवल यजुर्वेद से तथा दर्शपौर्णमासादि यज्ञ ऋग्वेद एवं यजुर्वेद से सम्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार सोमयज्ञ में तीनों वेदों से सम्बन्धित ऋत्विजों का वरण किया जाता है। सोमयज्ञ के चार प्रकार कहे गए हैं – एकाह, अहीन, साद्यस्क एवं सत्र। दीक्षा और उपसद् आदि के अनेक दिनों में सम्पन्न होने पर भी एक दिन में सम्पन्न होने वाले सोम याग को एकाह कहते हैं। दो सेलेकर बारह दिनों में सम्पादित होने वाले याग को अहीन याग कहते हैं। बारह से अधिक दिनों में सम्पादित सोमयज्ञ की संज्ञा सत्रयाग है। एक दिन में ही दीक्षा से आरम्भ कर अवभृथ पर्यन्त सारे कार्य सम्पन्न हों वह सोमयज्ञ साद्यस्क्र याग कहलाता है।
सोम रस बनाने की प्रक्रिया वैदिक यज्ञों में बड़े महत्व की है। इसकी तीन अवस्थाएं हैं- पेरना, छानना और मिलाना। वैदिक साहित्य में इसका पूरा वर्णन लिखा हुआ है। सोम के डंठलों को पत्थरों से कूट-पीसकर तथा भेड़ के ऊन की छलनी से छानकर प्राप्त किए जाने वाले सोमरस के लिए इंद्र, अग्नि ही नहीं और भी वैदिक देवता लालायित रहते हैं, तभी तो पूरे विधान से होम (सोम) अनुष्ठान में पण्डित सबसे पहले इन देवताओं को सोमरस अर्पित करते थे। बाद में प्रसाद के तौर पर लेकर खुद भी खुश हो जाते थे।
यद्यपि सोमयज्ञ के अङ्गरूप में बहुत सी इष्टियों का सम्पादन किया जाता है फिर भी इसका प्रधान द्रव्य सोम होने के कारण इसके लिए सोमयज्ञ शब्द प्रयोग किया जाता है। सोमयज्ञ की सात संस्थाएं हैं- अग्निष्टोम, अत्याग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र एवं आप्तोर्याम (वाजपेय)13 सोमयाग मेंजिस स्तोम से याग की समाप्ति होती है, उसी के आधार पर उस याग का नामकरण किया जाता है। अग्निष्टोमस्तोम के द्वारा समाप्ति होने के कारण अग्निष्टोम सोमयज्ञ कहलाता है। इसी प्रकार उक्थ्य, षोडशी और अतिरात्र संज्ञक स्तोमों की समाप्ति पर उक्थ्य आदि सोम संस्थाओं का नामकरण हुआ है।
सोमयज्ञ में मुख्य रूप से चार ऋत्विज्होते हैं (ब्रह्मा, उद्गाता, होता, अध्वर्यु) इन चारों ऋत्विजों के तीन-तीन सहायक पुरोहित होते हैं। इस प्रकार सोम याग में कुल सोलह ऋत्विज होते हैं।
सोमरस की जगह पंचामृत
आजकल सोमरस की जगह पंचामृत ने ले ली है, जो सोम की प्रतीति-भर है। कुछ प्राचीन धर्मग्रंथों में देवताओं को सोम न अर्पित कर पाने की स्तिथि में कोई और चीज अर्पित करने पर क्षमा- याचना करने के मंत्र भी लिखे हैं।
मुश्किल होती गई सोम की पहचान
अध्ययनों से पता चलता है कि वैदिक काल के बाद यानी ईसा के काफी पहले ही इस वनस्पति की पहचान मुश्किल होती गई। ऐसा भी कहा जाता है कि सोम (होम) अनुष्ठान करने वाले लोगों ने इसकी जानकारी आम लोगों को नहीं दी, उसे अपने तक ही सीमित रखा और आजकल ऐसे अनुष्ठानी लोगों की पीढ़ी/परंपरा के लुप्त होने के साथ ही सोम की पहचान भी मुश्किल होती गई।
सोमरस का उल्लेख- शास्त्रों में लिखे हैं सोम के कई चमत्कारी गुण

अनेक स्थलों पर मिलता है। सोमरस की औषधियों को श्रेष्ठ माना गया है। ऋग्वेद में सोमरस के बारे में कई जगह लिखा है। एक जगह पर सोम की इतनी उपलब्धता और प्रचलन दिखाया गया है कि इंसानों के साथ-साथ गायों तक को सोमरस भरपेट खिलाए और पिलाए जाने की बात कही गई है।
वैदिक ऋषियों का चमत्कारी आविष्कार सोमरस एक ऐसा पदार्थ है, जो संजीवनी की तरह कार्य करता है। यह जहां व्यक्ति की जवानी बरकरार रखता है वहीं यह पूर्ण सात्विक, अत्यंत बलवर्धक, आयुवर्धक व भोजन-विष के प्रभाव को नष्ट करने वाली औषधि है।
ऋग्वेद में लिखा है-
“स्वादुष्किलायं मधुमां उतायम्, तीव्र: किलायं रसवां उतायम।
उतोन्वस्य पपिवांसमिन्द्रम, न कश्चन सहत आहवेषु”
यानी की : सोम बड़ी स्वादिष्ट है, मधुर है, रसीली है। इसका पान करने वाला बलशाली हो जाता है। वह अपराजेय बन जाता है।
श्रीमद् भगवद्गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है,
त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते |
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्र्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् || ।।9.20।।
“जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं | वे पापकर्मों से शुद्ध होकर, इन्द्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनन्द भोगते हैं |”
शास्त्रों में सोमरस लौकिक अर्थ में एक बलवर्धक पेय माना गया है, परंतु इसका एक पारलौकिक अर्थ भी देखने को मिलता है। साधना की ऊंची अवस्था में व्यक्ति के भीतर एक प्रकार का रस उत्पन्न होता है जिसको केवल ज्ञानीजन ही जान सकते हैं।
ब्राह्मण ग्रन्थों में इसकी निर्माण विधि बताई गई है। सोमरस बनाने हेतु इसे धोकर कटा पीसा जाता था तथा रस निचौड लिया जाता था। सोम को कटते समय मंत्र उच्चारण का उल्लेख भी था।
कल्कि कृत सोमरस को मिट्टी या धातु के पात्र में रखते थे। बाद में जल मिलाकर वस्त्र से छानने के बाद इसको बूंद-बूंद के रूप में लोगों कोऔषध के रूप में दिया जाता था।
सोम का सम्बन्ध अमरत्व से भी है । वह स्वयं अमर तथा अमरत्व प्रदान करने वाला है । वह पितरों से मिलता है और उनको अमर बनाता है। कहीं-कहीं उसको देवों का पिता कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि वह उनको अमरत्व प्रदान करता है। अमरत्व का सम्बन्ध नैतिकता से भी है । वह विधि का अधिष्ठान और ॠत की धारा है वह सत्य का मित्र है।
आयुर्वेदिक ग्रंथ सोमरस के बारे में सूचना देते हैं- धन्वन्तरी सोमरस
रसेंद्रचूड़ामणि 6।6-9 में कहा है,
पञ्चांगयुक्पञ्चदशच्छदाढ्या सर्पाकृतिः शोणितपर्वदेशा।
सा सोमवल्ली रसबन्धकर्म करोति एकादिवसोपनीता।।
करोति सोमवृक्षोऽपि रसबन्धवधादिकम्।
पूर्णिमादिवसानीतस्तयोर्वल्ली गुणाधिका।।
कृष्ण पक्षे प्रगलति दलं प्रत्यहं चैकमेकं शुक्लेऽप्येकं प्रभवति पुनर्लम्बमाना लताः स्युः।
तस्याः कन्द: कलयतितरां पूर्णिमायां गृहीतो बद्ध्वा सूतं कनकसहितं देहलोहं विधत्ते।।
इयं सोमकला नाम वल्ली परमदुर्लभा।
अनया बद्धसूतेन्द्रो लक्षवेधी प्रजायते।
जिसके पंद्रह पत्ते होते हैं, जिसकी आकृति सर्प की तरह होती है। जहाँ से पत्ते निकलते हैं- वे गठिं जिसकी लाल होती है, ऐसी वह पूर्णिमा के दिन लायी हुई पञ्चांग (मूल, डण्डी, पत्ते, फूल और फल) से युक्त सोमवल्ली पारद को वद्ध कर देती है। पूर्णिमा के दिन लाए हुआ पञ्चांग से युक्त सोमवृक्ष भी पारद को बधिना, पारद की भस्म बनाना आदि कार्य कर देता है। परंतु सोमवल्ली और सोमवृक्ष, इन दोनों में सोमवल्ली अधिक गुणों वाली है।
इस सोमवल्ली का कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक-एक पत्ता झड़ जाता है। और शुक्ल पक्ष में पुनः प्रतिदिन एक-एक पत्ता निकल आता है। इस तरह यह लता बढ़ती रहती है। पूर्णिमा के दिन इस लता का कंद निकाला जाए तो वह बहुत श्रेष्ठ होता है। धतूरे के सहित इस कन्द में बँधा हुआ पारद देह को लोहे की तरह दृढ़ बना देता है। और इससे बँधा हुआ पारद लक्षवेधी हो जाता है अर्थात एक गुणाबद्ध पारद लाख गुणा लोहे को सोना बना देता है। यह सोम नाम की लता अत्यन्त ही दुर्लभ है। कम से कम आज के समय में सोमवल्ली किसी सोमलता से कम नहीं।
कण्व ऋषियों ने मानवों पर सोम का प्रभाव इस प्रकार बतलाया है- ‘यह शरीर की रक्षा करता है, दुर्घटना से बचाता है, रोग दूर करता है, विपत्तियों को भगाता है, आनंद और आराम देता है, आयु बढ़ाता है और संपत्ति का संवर्द्धन करता है। इसके अलावा यह विद्वेषों से बचाता है, शत्रुओं के क्रोध और द्वेष से रक्षा करता है,
कण्व ऋषियों के अनुसार सोमरस उल्लासपूर्ण विचार उत्पन्न करता है, पाप करने वाले को समृद्धि का अनुभव कराता है, देवताओं के क्रोध को शांत करता है और अमर बनाता है’। सोम विप्रत्व और ऋषित्व का सहायक है। सोम अद्भुत स्फूर्तिदायक, ओजवर्द्धक तथा घावों को पलक झपकते ही भरने की क्षमता वाला है, साथ ही आनंद की अनुभूति कराने वाला है।
सोमरस देव और मानव दोनों को यह रस स्फुर्ति और प्रेरणा देने वाला था । देवता सोम पीकर प्रसन्न होते थे; इन्द्र अपना पराक्रम सोम पीकर ही दिखलाते थे । कण्व ॠषियों ने मानवों पर सोम का प्रभाव इस प्रकार बतलाया है: ‘ यह शरीर की रक्षा करता है, दुर्घटना से बचाता है; रोग दूर करता है; विपत्तियों को भगाता है; आनन्द और आराम देता है; आयु बढ़ाता है।




















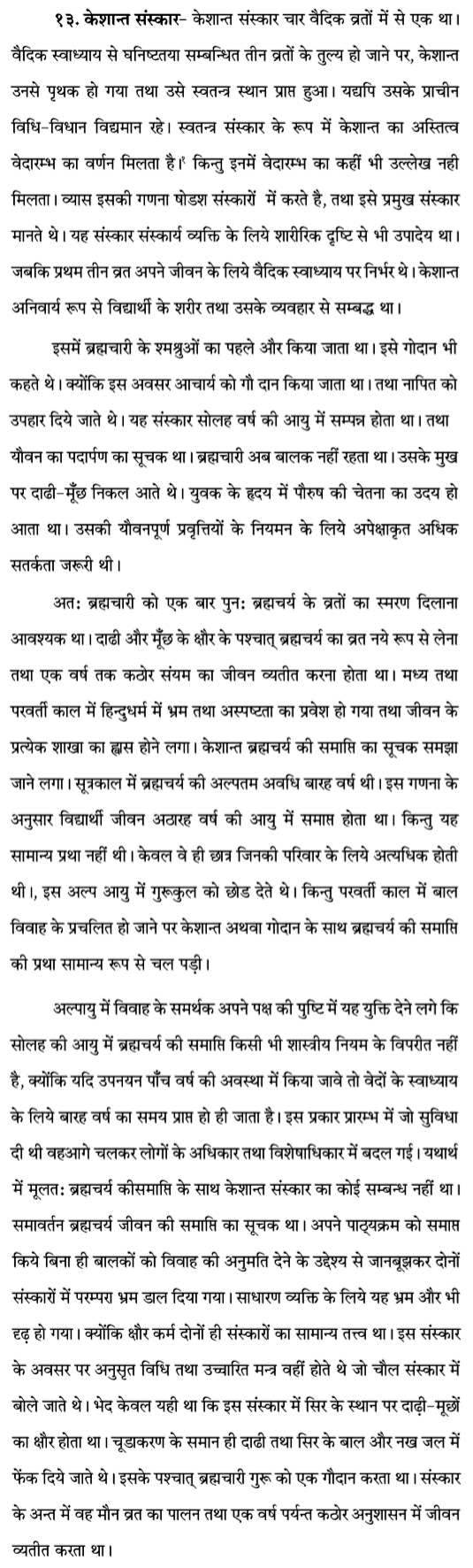

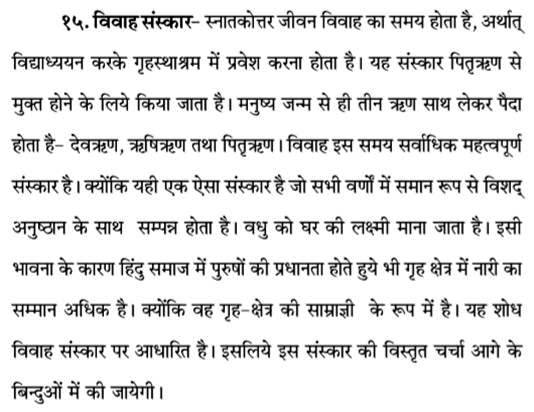




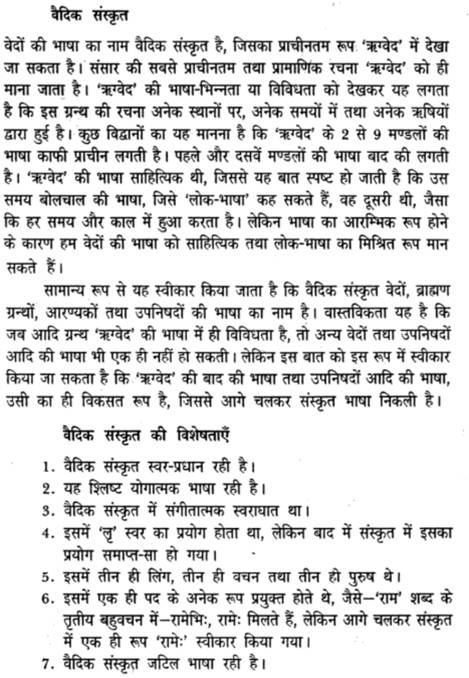
 सोत्र- हिंदी भाषा का स्वरूप विकास
सोत्र- हिंदी भाषा का स्वरूप विकास जिसकी ध्वन्यात्मक विशेषतायें उत्तर-पश्चिमी भारत के शिलालेखों में बहुत सीमा तक सुरक्षित है। मूलरूप में यह ब्राहमण धर्म की भाषा थी, जो उसी उत्तर पश्चिमी भाग से प्रचालितहुआ था। ब्राहमण धर्म के प्रसार के साथ इसका भी प्रसार हुआ और जब भारत के अन्य दो बड़े धर्म-जैन और बौद्ध धर्म फैलने लगे, तब कुछ समय के लिए इसका प्रसार रुक गया। जब भारत में दोनों धर्मों का अपकर्ष प्रारंभ हुआ तब इसने निर्विघ्न उन्नति करना प्रारम्भ किया धीरे-धीरे यह सारे भारत वर्ष में फैलने लगी। गुप्त काल को सांस्कृतिक विकास में भारत के स्वर्ण युग तथा सर्वोच्च और सबसे उत्कृष्ट समय के रूप में भी माना जाता है। गुप्त वंश के शासकों ने संस्कृत साहित्य को संरक्षित किया और उन्होंने उदारता से संस्कृत विद्वानों और कवियों की मदद की। अंततः संस्कृत भाषा सुसंस्कृत और शिक्षित लोगों की भाषा बन गई। इस दौर में कालिदास संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाटककार थे। कालिदास ने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की। इसमें अभिज्ञानशाकुन्तलम्, रघुवंशम्, कुमारसंभवम्; मेघदूतम् और ऋतुसंहार प्रमुख हैं। समय पाकर तो यह एक विशाल राष्ट्रीय भाषा बन गयी और केवल तभी यह पदच्युत हुई जब मुस्लिम शासकों का भारत में आगमन हुआ।
जिसकी ध्वन्यात्मक विशेषतायें उत्तर-पश्चिमी भारत के शिलालेखों में बहुत सीमा तक सुरक्षित है। मूलरूप में यह ब्राहमण धर्म की भाषा थी, जो उसी उत्तर पश्चिमी भाग से प्रचालितहुआ था। ब्राहमण धर्म के प्रसार के साथ इसका भी प्रसार हुआ और जब भारत के अन्य दो बड़े धर्म-जैन और बौद्ध धर्म फैलने लगे, तब कुछ समय के लिए इसका प्रसार रुक गया। जब भारत में दोनों धर्मों का अपकर्ष प्रारंभ हुआ तब इसने निर्विघ्न उन्नति करना प्रारम्भ किया धीरे-धीरे यह सारे भारत वर्ष में फैलने लगी। गुप्त काल को सांस्कृतिक विकास में भारत के स्वर्ण युग तथा सर्वोच्च और सबसे उत्कृष्ट समय के रूप में भी माना जाता है। गुप्त वंश के शासकों ने संस्कृत साहित्य को संरक्षित किया और उन्होंने उदारता से संस्कृत विद्वानों और कवियों की मदद की। अंततः संस्कृत भाषा सुसंस्कृत और शिक्षित लोगों की भाषा बन गई। इस दौर में कालिदास संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाटककार थे। कालिदास ने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की। इसमें अभिज्ञानशाकुन्तलम्, रघुवंशम्, कुमारसंभवम्; मेघदूतम् और ऋतुसंहार प्रमुख हैं। समय पाकर तो यह एक विशाल राष्ट्रीय भाषा बन गयी और केवल तभी यह पदच्युत हुई जब मुस्लिम शासकों का भारत में आगमन हुआ। द्वारा बोली गई ध्वनियां नहीं हैं। धरती और ब्रह्मांड में गति सर्वत्र है। चाहे वस्तु स्थिर हो या गतिमान। गति होगी तो ध्वनि निकलेगी। ध्वनि होगी तो शब्द निकलेगा। देवों और ऋषियों ने उक्त ध्वनियों और शब्दों को पकड़कर उसे लिपि में बांधा और उसके महत्व और प्रभाव को समझा।
द्वारा बोली गई ध्वनियां नहीं हैं। धरती और ब्रह्मांड में गति सर्वत्र है। चाहे वस्तु स्थिर हो या गतिमान। गति होगी तो ध्वनि निकलेगी। ध्वनि होगी तो शब्द निकलेगा। देवों और ऋषियों ने उक्त ध्वनियों और शब्दों को पकड़कर उसे लिपि में बांधा और उसके महत्व और प्रभाव को समझा।